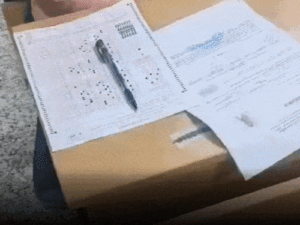शास्त्रीय होते हुए भी कोई तबला उस्ताद या पंडित या महाराज आम लोगों में इतना पॉपुलर नहीं हो सका जितना ज़ाकिर हुए। गुदई महाराज (पंडित सामता प्रसाद), किशन महाराज और ज़ाकिर के खुद के पिता उस्ताद अल्लारखा जैसे नामी तबला वादक भी नहीं। वर्षों ये बात हर शहर और गाँव में आम थी कि घरों, दफ़्तरों में कोई टेबल या पटिया ठोंकते दिख जाए तो कहा जाता था- चल- चल ज़ाकिर हुसैन मत बन। जहां तक तबला में उनकी उस्तादी की बात है तो वे सबसे अलग थे। बडे- बड़े उस्ताद और पंडित पुराने क़ायदे या परन ही बजाते थे। उनमें कुछ सुधार या नया खटका भी ले आते थे लेकिन ज़ाकिर हमेशा कुछ नया करते थे। जैसे उनमें किसी भी ताल में कहीं से भी तिहाई मारने की क्षमता थी और वे ऐसा करते भी थे। उन्होंने अपने पिता के साथ जुगलबंदी तो की ही, शास्त्रीय संगीत की चार पीढ़ियों के साथ संगत भी की। पंडित रविशंकर, पंडित जसराज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिवकुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली और पिया बसंती रे… गाने वाले सारंगी उस्ताद सुल्तान खां साहब के बाद उनके बेटे साबिर खां के साथ भी उन्होंने तबला बजाया। उनकी उँगलियाँ, जैसे साक्षात ईश्वर। कभी इन उँगलियों पर तबला के जरिए मदमाता हाथी आता था। कभी विश्वनाथ मंदिर से टकराती गंगा मैया का वैग तो कभी बनारस की गलियों में घूमते लोग भी आते थे। मंदिर का घंटा, झाँझ- मंजीरे, ढोल और शंख ध्वनि भी वे एक साथ तबला से निकाल देते थे। परन और रेलों में उनकी उँगलियाँ ऐसे चलती थीं जैसे पानी का रेला हो या कोई झरना हो। वे राधा का ग़ुस्सा भी क़ायदे में बताते थे। उनके घुँघरुओं को परन में उकेरते थे और कृष्ण की लीला भी कभी बाएँ तो कभी दाएँ से समझाते थे। कितनी ही तेज रफ़्तार में आप उनकी हर उँगली को अलग सुन सकते थे। यही उस्ताद का कमाल था। बड़े और छोटे ख़्याल की शास्त्रीयता के साथ हवेली संगीत और लोक गीतों पर भी उन्होंने वही ताल दी जो लोक की माँग होती है या भजन के भाव होते हैं।